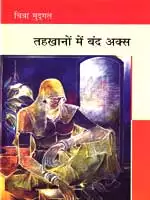|
कहानी संग्रह >> तहखानों में बंद अक्स तहखानों में बंद अक्सचित्रा मुदगल
|
382 पाठक हैं |
|||||||
सुपरिचित वरिष्ठ कथाकार-विचारक चित्रा मुद् गल की एक नई कृति...
देश-विदेश में अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता, सरोकारों और
नारी-अस्मिता के लिए समर्पित लेखन के लिए सुपरिचित वरिष्ठ कथाकार-विचारक
चित्रा मुद्गल की नई कृति ‘तहखानों में बंद अक्स’ स्त्री-विमर्श के बने-बनाए फ्रेम से एकदम अलग एक पठनीय कृति है।
समाज-सेवा से मिले व्यापक अनुभवों ने उन्हें ‘झुग्गी-झोपड़ियों में प्रेम’ को देखने की आत्मीय दृष्टि प्रदान की है, तो वह दूसरी औरत को भी समाज में बेगैरत नहीं मानतीं। सामाजिक समता का राग अलापने वाले समाज से वह आंख में आंख डालकर जो प्रश्न करती हैं, उससे हमारा ढोंगी समाज बेनकाब हो जाता है।
उनकी दृष्टि में स्त्री आज अपने लिए एक सम्मानजनक जगह चाहती है, रियायत नहीं। उनकी नजर समाज के हर वर्ग पर रहती है और उन दबावों पर भी जो आज युवतियों पर पड़ रहे हैं। वह उन्हें भयमुक्त करते हुए सहज जीवन की राह दिखाती हैं।
इस पुस्तक को पढ़ने वाली युवतियां न तो सड़कछाप मजनुओं से डरेंगी और न दहेज जैसी बुराइयों का सामना करने से। वह एक बेहतर पत्नी और मां तो बनेगी ही, उनमें सही सोच का निरंतर विस्तार भी होगा।
चित्राजी की कहानियों की तरह ये लेख भी पाठकों से अपना एक सीधा रिश्ता बनाते हैं। ‘तहखानों में बंद अक्स’ एक संग्रहणीय पुस्तक है।
समाज-सेवा से मिले व्यापक अनुभवों ने उन्हें ‘झुग्गी-झोपड़ियों में प्रेम’ को देखने की आत्मीय दृष्टि प्रदान की है, तो वह दूसरी औरत को भी समाज में बेगैरत नहीं मानतीं। सामाजिक समता का राग अलापने वाले समाज से वह आंख में आंख डालकर जो प्रश्न करती हैं, उससे हमारा ढोंगी समाज बेनकाब हो जाता है।
उनकी दृष्टि में स्त्री आज अपने लिए एक सम्मानजनक जगह चाहती है, रियायत नहीं। उनकी नजर समाज के हर वर्ग पर रहती है और उन दबावों पर भी जो आज युवतियों पर पड़ रहे हैं। वह उन्हें भयमुक्त करते हुए सहज जीवन की राह दिखाती हैं।
इस पुस्तक को पढ़ने वाली युवतियां न तो सड़कछाप मजनुओं से डरेंगी और न दहेज जैसी बुराइयों का सामना करने से। वह एक बेहतर पत्नी और मां तो बनेगी ही, उनमें सही सोच का निरंतर विस्तार भी होगा।
चित्राजी की कहानियों की तरह ये लेख भी पाठकों से अपना एक सीधा रिश्ता बनाते हैं। ‘तहखानों में बंद अक्स’ एक संग्रहणीय पुस्तक है।
अनुक्रम
आवाजों को गुहराती आवाजें
बिना फ्रेम के कुछ दृश्य अंतरचेतना की अदृश्य
पिटारी में
कुछ इस तरह से स्थिर हो जाते हैं कि बीत गए और बीतते समय के काले अंधड़ भी
उन्हें, अपनी कील से उखाड़ नहीं पाते।
विस्मय होता है कि वे धुंधला तक नहीं पाए। शायद कोई रहस्यमय भीति, उन्होंने स्वयं अपने इर्द-गिर्द चुन रखी है। ताकि सुरक्षित रह सके स्त्री का छलनी हुआ अस्तित्व। ताकि जब भी उसे देखना हो अपने भूगोल और इतिहास की लहू रिसती सांधों को अविचलित देख सके वह उन दृश्यों को गौर से। बन सके स्वयं ही स्वयं के लिए साक्षी। क्योंकि सच के झुलसा देने वाले ताप को सह पाना सामान्यजन के बूते का नहीं। उनके बूते का तो हरगिज नहीं जो उत्तरदायी हैं उसके ‘स्व’ को अनदेखा करने के लिए।
एक ऐसा ही दृश्य जहन में कभी-कभी आंखें खोलता है और विवश करता है अपनी ओर देखने के लिए।
गांव वाले घर की बाई खमसार के अंतिम छोर पर छत तक उठी, काली नक्काशीदार अलमारी के उस पार अवस्थित अपने अंधेरे कुप्प कमरे के भीतर, काठ के भारी-भरकम संदूक के ऊपर चढ़े संदूक पर रखे अपने सिंगार पिटारे से कंघी और आईना निकालकर अम्मा, ढिबरी की कांपती मटियाली उजास में अपने बाल संवारती हैं। मांग भरती हैं। आंखों में काजल आंजती हैं। माथे पर टिकुली टांकती हैं।
आखिरी बार आई में दाएं-बाएं कोणों से अपनी छवि निहारकर वे छवि समेत आइने को वापस सिंगार पिटारे में सहेज देती हैं।
पीठ पर झूल रहे अपने आंचल को सिर पर टिका, आंचल को नाक तक खींच लेती हैं।
फिर फूंक खाई ढिबरी को कमरे के भीतर के आले के हवाले कर माचिस मुट्ठी में चांप कमरे से बाहर आकर अम्मा किवाड़ों की सांकल चढ़ा देती हैं।
कायदा नहीं है उस घर का। उस घर का ही नहीं स्त्री की अंधेरी दुनिया के अधिकांश अंतरे-कोनों का। दिन के उजाले में घर की बहू मजाल कि सिर से पल्ला हटा आईने में अपना रूप निहार ले।
एक मुलाकात में मैंने डॉक्टर धर्मवीर भारतीजी से कहा था। उन आईनों को मैं सिंगार पिटारे के अंधेरे तहखानों से मुक्त करना चाहती हूं। लेकिन हां, अपनी पारंपरिक छवि से स्त्री को उन आईनों से अगर कोई मुक्त कर सकता है तो वह औरत स्वयं।
गांव से निकलते ही आरंभ हुई थी अम्मा की दूसरी दुनिया। वह महानगर था आज का चेन्नई, कल का मद्रास।
जहां पहुंचकर उनकी स्त्री उन प्रतिबंधों से किसी सीमा तक मुक्त हुई और अपना रूप दिन के उजाले में देख पाने के लिए स्वतंत्र। लेकिन इतनी-सी स्वतंत्रता क्या उस स्त्री को तहखानों के उन अंधेरों से मुक्त कर पाई जो अंधेरे, चतुराई और छल से उसके लिए सामाजिक सुव्यवस्था की बिसात की आड़ में, सुरक्षा और संरक्षण के निमित निर्मित किए गए थे।
तार्किकता के साथ कि कोमल तनया वामा स्वयं की सुरक्षा में सर्वथा अक्षम है। फिकरे कुछ और भी हैं, चुभते हुए।
कंठ तो है उसके पास मगर, आवाज नहीं है।
मस्तिष्क भी है मगर, चेतना नहीं।
बदलते समय में उसके अस्तित्व को चुनौती देते उन मुद्दों की असलियत क्या है जो सामाजिक संक्रमण से उपजे हैं, उपज रहे हैं और निरंतर उसके विरुद्ध विसंगतियां उगल रहे हैं। मार इकतरफा नहीं है। कुछ मुद्दे और हैं। जो स्वयं स्त्री के द्वारा स्त्री के लिए पैदा किए गए हैं। स्त्री स्वायतत्ता और ‘स्पेस’ के भ्रम में। जो उससे उसका स्पेस किसी न किसी बहाने छीन रहे हैं। वह अनजान है। सोच नहीं पा रही है। स्त्री को स्त्री के विरुद्ध खड़ा करने में किनकी स्वार्थसिद्धि है!
स्त्री की उपस्थिति के आयतन को उस अनुपस्थिति में भी उपस्थित देखा, महसूसा जा सकता है। जिन समकालीन मुद्दों में उसकी साझीदारी की जरूरत नहीं समझी गई है।
उसकी आवाज है। वह बोल नहीं रही थी। क्योंकि उससे कभी कुछ पूछा ही नहीं गया। पूछा जाता है तो मामूली-सी उकसाहट उसके भीतर दबे-जमे लावे को इस कदर खदबदा देती है कि उसके उफान को रोका नहीं जा सकता। गहरे प्रतीति दिलाती है वह कि संवेदना और सहिष्णुता से आवृत्त उसकी प्रखर तार्किकता समय की मांग के अनुरूप स्वयं को बदलने में सक्षम है। उसे अनुमान है। कभी वह अपने समय के साथ चल नहीं पाई थी। उसका समय निर्ममता से उसे पीछे छोड़ खुद आगे बढ़ गया था। अब वह समय से होड़ लेने की कोशिश कर रही है।
डॉ. भारती ने ‘धर्मयुग’ में लगातार इन कथात्मक रिर्पोताजों का प्रमुखता से प्रकाशन कर मुझसे ज्यादा उनकी आवाज़ों को मंच प्रदान किया, जिनके मत हाशिए पर भी सदैव उपेक्षित ही रहे। एक-एक लेख के लिए तीन-चार पृष्ठों तक की खुली गुंजाइश मामूली उत्साहवर्धन नहीं होता। पाठकों की सहमति-असहमति से भरी उत्तेजक प्रतिक्रियाओं ने मूल पाठ के अंतर्निहित विमर्श को निर्भीकता पूर्वक रेशे-रेशे उद्घाटित ही नहीं किया, बल्कि अपने समय काल से जोड़कर उसकी दूरगामी संगति-विसंगति को समाज विज्ञानी दृष्टि से पोस्टमार्टम भी किया।
अपनी सर्जना सामर्थ्य के प्रति भी मैं कभी बहुत आश्वस्त नहीं रही। अब भी नहीं हूं।
इतना जरूर कह सकती हूं। कुछ दिमागी जालों को निश्चय ही साफ करने की जरूरत है।
आमजन की पैरवी करने वालों के दोहरेपन ने कई दफे इन लेखों की प्रतिक्रिया में अपने कटाक्ष से पीड़ा पहुंचाई है। वे मानकर चलते हैं कि गंभीर सामाजिक समस्याओं पर सोच सकने की सामर्थ्य केवल बुद्धिजीवी वर्ग को ही हासिल है। वे समाज के नियंता सेलीब्रिटीज हैं। उन आमजन के लिए वे बेहतर सोच पाते हैं जिन्हें अपने लिए सोचने की कभी आदत नहीं रही। उनके दुखों से अंशतः सहमत होते हुए भी इस दंभ से सहमत होना कतई मुमकिन नहीं कि आमजन उनके संपर्क में कितना और कहां तक है?
किसी भी अति प्रतीक्षित पुस्तक का प्रकाशन उसके लेखक के लिए प्रीतिकर अनुभूति होती है। पहली पछुआ की छुअन से मंद-मंद हिलोरे लेती झील की आत्मावस्थित जल सतह-सी।
विस्मय होता है कि वे धुंधला तक नहीं पाए। शायद कोई रहस्यमय भीति, उन्होंने स्वयं अपने इर्द-गिर्द चुन रखी है। ताकि सुरक्षित रह सके स्त्री का छलनी हुआ अस्तित्व। ताकि जब भी उसे देखना हो अपने भूगोल और इतिहास की लहू रिसती सांधों को अविचलित देख सके वह उन दृश्यों को गौर से। बन सके स्वयं ही स्वयं के लिए साक्षी। क्योंकि सच के झुलसा देने वाले ताप को सह पाना सामान्यजन के बूते का नहीं। उनके बूते का तो हरगिज नहीं जो उत्तरदायी हैं उसके ‘स्व’ को अनदेखा करने के लिए।
एक ऐसा ही दृश्य जहन में कभी-कभी आंखें खोलता है और विवश करता है अपनी ओर देखने के लिए।
गांव वाले घर की बाई खमसार के अंतिम छोर पर छत तक उठी, काली नक्काशीदार अलमारी के उस पार अवस्थित अपने अंधेरे कुप्प कमरे के भीतर, काठ के भारी-भरकम संदूक के ऊपर चढ़े संदूक पर रखे अपने सिंगार पिटारे से कंघी और आईना निकालकर अम्मा, ढिबरी की कांपती मटियाली उजास में अपने बाल संवारती हैं। मांग भरती हैं। आंखों में काजल आंजती हैं। माथे पर टिकुली टांकती हैं।
आखिरी बार आई में दाएं-बाएं कोणों से अपनी छवि निहारकर वे छवि समेत आइने को वापस सिंगार पिटारे में सहेज देती हैं।
पीठ पर झूल रहे अपने आंचल को सिर पर टिका, आंचल को नाक तक खींच लेती हैं।
फिर फूंक खाई ढिबरी को कमरे के भीतर के आले के हवाले कर माचिस मुट्ठी में चांप कमरे से बाहर आकर अम्मा किवाड़ों की सांकल चढ़ा देती हैं।
कायदा नहीं है उस घर का। उस घर का ही नहीं स्त्री की अंधेरी दुनिया के अधिकांश अंतरे-कोनों का। दिन के उजाले में घर की बहू मजाल कि सिर से पल्ला हटा आईने में अपना रूप निहार ले।
एक मुलाकात में मैंने डॉक्टर धर्मवीर भारतीजी से कहा था। उन आईनों को मैं सिंगार पिटारे के अंधेरे तहखानों से मुक्त करना चाहती हूं। लेकिन हां, अपनी पारंपरिक छवि से स्त्री को उन आईनों से अगर कोई मुक्त कर सकता है तो वह औरत स्वयं।
गांव से निकलते ही आरंभ हुई थी अम्मा की दूसरी दुनिया। वह महानगर था आज का चेन्नई, कल का मद्रास।
जहां पहुंचकर उनकी स्त्री उन प्रतिबंधों से किसी सीमा तक मुक्त हुई और अपना रूप दिन के उजाले में देख पाने के लिए स्वतंत्र। लेकिन इतनी-सी स्वतंत्रता क्या उस स्त्री को तहखानों के उन अंधेरों से मुक्त कर पाई जो अंधेरे, चतुराई और छल से उसके लिए सामाजिक सुव्यवस्था की बिसात की आड़ में, सुरक्षा और संरक्षण के निमित निर्मित किए गए थे।
तार्किकता के साथ कि कोमल तनया वामा स्वयं की सुरक्षा में सर्वथा अक्षम है। फिकरे कुछ और भी हैं, चुभते हुए।
कंठ तो है उसके पास मगर, आवाज नहीं है।
मस्तिष्क भी है मगर, चेतना नहीं।
बदलते समय में उसके अस्तित्व को चुनौती देते उन मुद्दों की असलियत क्या है जो सामाजिक संक्रमण से उपजे हैं, उपज रहे हैं और निरंतर उसके विरुद्ध विसंगतियां उगल रहे हैं। मार इकतरफा नहीं है। कुछ मुद्दे और हैं। जो स्वयं स्त्री के द्वारा स्त्री के लिए पैदा किए गए हैं। स्त्री स्वायतत्ता और ‘स्पेस’ के भ्रम में। जो उससे उसका स्पेस किसी न किसी बहाने छीन रहे हैं। वह अनजान है। सोच नहीं पा रही है। स्त्री को स्त्री के विरुद्ध खड़ा करने में किनकी स्वार्थसिद्धि है!
स्त्री की उपस्थिति के आयतन को उस अनुपस्थिति में भी उपस्थित देखा, महसूसा जा सकता है। जिन समकालीन मुद्दों में उसकी साझीदारी की जरूरत नहीं समझी गई है।
उसकी आवाज है। वह बोल नहीं रही थी। क्योंकि उससे कभी कुछ पूछा ही नहीं गया। पूछा जाता है तो मामूली-सी उकसाहट उसके भीतर दबे-जमे लावे को इस कदर खदबदा देती है कि उसके उफान को रोका नहीं जा सकता। गहरे प्रतीति दिलाती है वह कि संवेदना और सहिष्णुता से आवृत्त उसकी प्रखर तार्किकता समय की मांग के अनुरूप स्वयं को बदलने में सक्षम है। उसे अनुमान है। कभी वह अपने समय के साथ चल नहीं पाई थी। उसका समय निर्ममता से उसे पीछे छोड़ खुद आगे बढ़ गया था। अब वह समय से होड़ लेने की कोशिश कर रही है।
डॉ. भारती ने ‘धर्मयुग’ में लगातार इन कथात्मक रिर्पोताजों का प्रमुखता से प्रकाशन कर मुझसे ज्यादा उनकी आवाज़ों को मंच प्रदान किया, जिनके मत हाशिए पर भी सदैव उपेक्षित ही रहे। एक-एक लेख के लिए तीन-चार पृष्ठों तक की खुली गुंजाइश मामूली उत्साहवर्धन नहीं होता। पाठकों की सहमति-असहमति से भरी उत्तेजक प्रतिक्रियाओं ने मूल पाठ के अंतर्निहित विमर्श को निर्भीकता पूर्वक रेशे-रेशे उद्घाटित ही नहीं किया, बल्कि अपने समय काल से जोड़कर उसकी दूरगामी संगति-विसंगति को समाज विज्ञानी दृष्टि से पोस्टमार्टम भी किया।
अपनी सर्जना सामर्थ्य के प्रति भी मैं कभी बहुत आश्वस्त नहीं रही। अब भी नहीं हूं।
इतना जरूर कह सकती हूं। कुछ दिमागी जालों को निश्चय ही साफ करने की जरूरत है।
आमजन की पैरवी करने वालों के दोहरेपन ने कई दफे इन लेखों की प्रतिक्रिया में अपने कटाक्ष से पीड़ा पहुंचाई है। वे मानकर चलते हैं कि गंभीर सामाजिक समस्याओं पर सोच सकने की सामर्थ्य केवल बुद्धिजीवी वर्ग को ही हासिल है। वे समाज के नियंता सेलीब्रिटीज हैं। उन आमजन के लिए वे बेहतर सोच पाते हैं जिन्हें अपने लिए सोचने की कभी आदत नहीं रही। उनके दुखों से अंशतः सहमत होते हुए भी इस दंभ से सहमत होना कतई मुमकिन नहीं कि आमजन उनके संपर्क में कितना और कहां तक है?
किसी भी अति प्रतीक्षित पुस्तक का प्रकाशन उसके लेखक के लिए प्रीतिकर अनुभूति होती है। पहली पछुआ की छुअन से मंद-मंद हिलोरे लेती झील की आत्मावस्थित जल सतह-सी।
चित्रा मुद्गल
मड़ैया में प्रेम
प्रेम की तमाम व्याख्याएं हैं और अब तक उसे
व्याख्यायित
किया जा रहा है। समय की करवट से प्रेम भी अछूता नहीं है। उसके ताप का
उत्ताप अनेकों रंग और स्पंदन का अबूझ रसायन है।
प्रेम का अर्थ उन महिलाओं के लिए क्या है जो अर्थाभाव और मशक्कत में जी रही हैं या जो आधुनिकता की चकाचौंध से नावाकिफ अब भी परंपराओं की कैद से बाहर नहीं देख पाई हैं, या जो मेहनत-मजदूरी में हाड़ तोड़ जिंदगी जी रही हैं, या जिन्हें उपेक्षिता होने का पैदाइशी हक मिला हुआ है?
तथाकथित आधुनिक नारी की प्रेम और सेक्स को लेकर अपनी व्याख्याएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, अभिव्यक्ति है, स्वीकारोक्ति है, आइए इन महिलाओं के प्रेम और सेक्स पर इनके दृष्टिकोण से परिचित हों।
‘जानती हो प्रेम क्या है?’
‘हऊ।’
‘क्या होता है?’
प्रेम का अर्थ उन महिलाओं के लिए क्या है जो अर्थाभाव और मशक्कत में जी रही हैं या जो आधुनिकता की चकाचौंध से नावाकिफ अब भी परंपराओं की कैद से बाहर नहीं देख पाई हैं, या जो मेहनत-मजदूरी में हाड़ तोड़ जिंदगी जी रही हैं, या जिन्हें उपेक्षिता होने का पैदाइशी हक मिला हुआ है?
तथाकथित आधुनिक नारी की प्रेम और सेक्स को लेकर अपनी व्याख्याएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, अभिव्यक्ति है, स्वीकारोक्ति है, आइए इन महिलाओं के प्रेम और सेक्स पर इनके दृष्टिकोण से परिचित हों।
‘जानती हो प्रेम क्या है?’
‘हऊ।’
‘क्या होता है?’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i